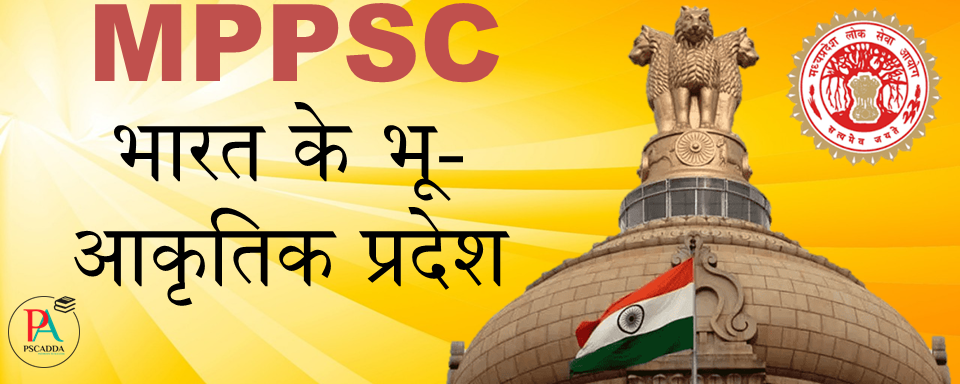भारत के भू-आकृतिक प्रदेश
देश के संरचना एवं भौतिक स्वरूप में काफी विविधता मिलती है।
देश में लगभग 10.6 प्रतिशत क्षेत्र पर पर्वत, 18.5 प्रतिशत क्षेत्र पर पहाड़ीयां, 27.7 प्रतिशत पर पठार और 43.2 प्रतिशत क्षेत्र पर विस्तृत मैदान है।
भारत को 5 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है।
- उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र
- उत्तर भारत का विशाल मैदान
- प्रायद्वीपीय पठारी भाग
- तटीय मैदान
- द्वीप समुह

उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र (हिमालय ) :-
- यह पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में उरूणाचल प्रदेश तक(2400- 2500 किमी.) में फैला हुआ है।
- इसकी चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा(2000 किमी.) पश्चिम में (500 किमी.) ज्यादा है।
- इसका कारण है पश्चिमी अपेक्षा पूर्व में दबाव-बल का अधिक होना।
- यह नवीन मोड़दार पर्वत माला है इसका आकार धनुष की भांती है।

हिमालय की स्थिती :-
देश के ऊपरी सीमांन्त के सहारे सिंन्धु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है।
हिमालय पर्वत का निर्माण यूरोशियाई प्लेट(अंगारा लैंड) और इंडो –आस्ट्रेलिया प्लेट(गोंडवाना लैंड ) के टकराने से टेथिस सागर के ऊपर हुआ है।
प्लेट-विवर्तनिकी सिंद्धान्त के पहले यह माना रहा था कि हिमालय की उत्पत्ति टेथीस सागर में जमें मलबों में दबाव पड़ने से हुआ है। अतः हम टेथीस सागर को ‘हिमालय का गर्भ-गृह’ कहते हैं।
यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, प्रथम अंटार्कटिका व द्वितीय आर्कटिक प्रदेश है।
उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को चार भागों में बांटा जा सकता है।
- ट्रांस हिमालय क्षेत्र
- वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय श्रेणी
- लघु या मध्य हिमालय श्रेणी
- उप हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी
1. ट्रांस हिमालय क्षेत्र :-
ट्रांस हिमालय को ‘तिब्बती हिमालय’ या ‘टेथीस हिमालय’ भी कहा जाता है इसकी लम्बाई 965 किमी.(लगभग) चौड़ाई 40 से 225 किमी.(लगभग) है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 3100 से 3700 मी. तक है। इस श्रेणी पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसके अन्तर्गत काराकोरम, कैलाश, जास्कर एवं लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का बना है यह श्रेणी सतलज , सिंधु व ब्रह्मपूत्र(सांगपो) जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है।
K2 या गाडविन आस्टिन(8611 मीटर ) :- भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी है जो काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है।
ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालयों से इंडो-सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होती है।

2. वृहद हिमालय :-
- इसे हिमालय या सर्वोच्च हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है।
- इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मी., लंम्बाई 2500 किमी. और चौड़ाई 25 किमी. है।
- यह पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचाबर्वा पर्वत तक फैला है।
- इसी श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटिंया पायी जाती है।
- जिनमें प्रमुख है – माउण्ट एवरेस्ट(8848 मी.), कंचनजंगा(8598 मी.), मकालू(8481मी.), धौलागिरी(8172मी.), नंगा पर्वत(8126 मी.), अन्नपूर्णा(8048 मी.), नंदा देवी(7817 मी.), नामचाबर्वा (7756 मी.) आदि।
- यह उत्तर में सिन्धु नदी के मोड से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है।
- सिन्धु, सतलज, दिहांग, गंगा, यमुना तथा इनकी सहायक नदियों की घाटियां इसी श्रेणी में स्थित है।
- वृहद हिमालय में पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। अर्थात पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक निचले भाग तक बर्फ देखी जा सकती है।
- माउण्ट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है। माउण्ट एवरेस्ट का नामकरण 1865 में भारत के महासर्वेक्षक जार्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया।
- एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुगंमा कहते थे। जिसका अर्थ है ‘पर्वतों की रानी’।
- इस श्रेणी में कई दर्रे भी मिलते हैं जिनमें प्रमुख हैं – जोजिला, बुर्जिल, बारालाचा, शिपकीला, नीति, लिपूलेख, नाथूला, जेलेपला आदि।
- इस श्रेणी में गंगा एवं यमुना नदियों का उद्गम स्थल भी है।
- इस श्रेणी में गंगोत्री हिमनद(उत्तराखण्ड), मिलाप एवं जम्मू हिमनद आदि प्रमुख हैं।
- वृहद हिमालय, लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है।
3. लघु हिमालय
- यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है।
- इसकी चौड़ाई 80 से 100 किमी. तथा औसत ऊंचाई 1800 से 300 मी. है।
- अधिकतम ऊंचाई 4500 मी. तक पायी गयी है।
- पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है।
- लघु हिमालय की सबसे प्रमुख एवं लम्बी श्रेणी पीरपंजाल श्रेणी है।
- पीरपंजाल श्रेणी झेलम और व्यास नदियों के बीच फैली है।
- इस श्रेणी में पीर पंजाल(3494 मी.) और बनिहाल(2832 मी.) दो प्रमुख दर्रे हैं।
- बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है।
- लघु हिमालय अपने स्वास्थवर्धक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है
- इसके अन्तर्गत चकरौता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एवं इल्हौजी नगर आते हैं।
- जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मी. के बीच पाई जाती है।
- इस श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे-छोटे घास के मैदानों का जम्मू-कश्मीर में मर्ग(जैसे – गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग) और उत्तराखंड में वुग्याल और पयार कहते हैं।
- लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फाल्ट के द्वारा अलग होती है।
4. उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी :-
- यह श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है
- इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान(पंजाब) के पोटवार बेसिन से पूर्व में कोसी नदी तक है।
- इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मी. के बीच है तथा चौड़ाई 10 से 50 किमी. तक है।
- शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में दून(जैसे – देहरादून) व पूरब में द्वार(जैसे – हरिद्वार) कहते हैं।
- यह हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है।
- शिवालिक श्रेणीयां मायो-प्लीस्टोसीन बालू कंकड तथा कांग्लोमेरिट शैल की मोटी परतों से बनी है।
- शिवालिक को जम्मू-कश्मीर में जम्मू पहाडि़यां तथा अरूणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अवोर और मिशमी की पहाडि़यों के नाम से जाना जाता है।
- शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश हैं।
- तराई से सटे दक्षिणी भाग में ग्रेट बाउंडरी फाल्ट मिलता है जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है।
हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन :-
सिडनी ब्रोनार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय क्षेत्र को प्रमुख 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है।

कश्मीर या पंजाब हिमालय – सिन्धु और सतलज नदियों के बीच फैला हुआ है।
यहां हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक होती है। यह लगभग 560 किमी. की दुरी में फैला हुआ है।
कुमायूं हिमालय – यह सतलज एवं काली (शारदा ) नदियों के बीच फैला हुआ है। यह लगभग उत्तराखण्ड क्षेत्र में वितृत है। (सबसे छोटा भाग )
नेपाल हिमालय – यह काली एवं तिस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है यहां हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है परन्तु हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि मिलते हैं। यह हिमालय का सबसे लम्बा एवं सर्वाधिक ऊंचाई वाला प्रादेशिक विभाग है।
असम हिमालय – यह तिस्ता एवं दिहांग(ब्रह्मपुत्र) नदियों के बीच फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख नदियां दिहांग, दिवांग, लोहित एवं ब्रह्मपुत्र नदियां है।
2. उत्तर का विशाल मैदान :-
- इस मैदान की अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच है।
- इसका निर्माण क्वार्टनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लोस्टीसीन एवं होलोसीन युग में हुआ है।
- हिमालय से निकलने वाली नदियां (जैसे – गंगा, यमुना, सिंधु, बह्मपुत्र आदि) तथा प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियां(सोन, चम्बल आदि) के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमा करते जाने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ।
- इसे सिन्धु-गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं।
- यह मैदान धनुषाकार रूप से 3200 किमी. में देश के 7.5 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र पर विस्तृत है।
- इसकी चौड़ाई पश्चिम में 480 किमी. तथा पूर्व में 145 किमी. है।
- अंबाला के आस-पास की भूमि इस मैदान में जल-विभाजक का कार्य करती है क्यौंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं।
- इस क्षेत्र में नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से यहां की भूमि उपजाऊ होती है। इसलिए इस क्षेत्र को भारत का अनाज का कटोरा कहा जाता है।

संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इसका विभाजन चार भागों में किया गया है।
- भाबर
- तराई प्रदेश
- बागर
- खादर
1. भाबर :-
भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिन्धु नदी से तीस्ता नदी के बीच पाया जाता है। यह क्षेत्र हिमालय तथा गंगा के बीच पाया जाता है। यह एक कंकड़ पत्थर वाला मैदान है इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई कंकड़ पत्थर के विक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इसे शिवालिक का जलौढ – पंख कहा जाता है। भाबर क्षेत्र में पहुंचकर अनेक नदियां भूमिगत हो जाती हैं।
2. तराई प्रदेश :-
इसका विस्तार भाबर के ठीक नीचे है उत्तराखण्ड से लेकर असोम तक विस्तृत इस प्रदेश की संरचना बारीक कंकड़-पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किमी. तक पायी जाती है यहां महीन रेत व चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। भाबर में लुप्त नदियां तराई प्रदेश में पुनः प्रकट हो जाती हैं। समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैल कर दलदल का निर्माण करता है। यह प्रदेश घने वनों से ढका था जिसे वर्तमान में काटकर कृषि भूमि में परिवर्तीत कर दिया गया है।
3. बांगर :-
यह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता। बांगर प्रदेश वह प्रदेश है जिसका निर्माण पुराने जलोढ़ से बाढ़ युक्त मैदानों से दूर होता है। सतलज के मैदान एवं गंगा मैदान गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता है। इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल एवं उच्च भूमि बन गई है। इस स्थानीय नाम भूंड दिया गया है। यह प्रदेश कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता।
4. खादर :-
यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बना है तथा अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहां नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है। अतः इस प्रदेश को ‘कछारी प्रदेश’ या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। यह प्रतिवर्ष बाढ़ों निक्षेपित होने वाला नविन जलोढ़क है। खादर प्रदेश का विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। उदाहरण – गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा।
यह प्रदेश कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। बिहार पुर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र जो नदी घाटियों से सटे हैं। खादर प्रदेश के अन्तर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खादर को खादव व पंजाब में इसे बेट कहते हैं।
उच्चावच की दृष्टि से उत्तर के विशाल के मैदान को निम्न लिखित उप विभागों में विभाजित किया गया है :-
1. पंजाब-हरियाणा का मैदान – इस क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः सतलज-रावी-व्यास के बीच का भूभाग है जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में स्थित है।
पश्चिम से पूर्व की ओर दोआबों का क्रम –
- सिन्धु-झेलम का -सिन्धु सागर दोआब
- झेलम-चेनाब का -चाज दोआब
- चेनाब-रावी का -रचना दोआब
- रावी-व्यास का -बारी दोआब
- व्यास-सतलज का -बिस्ट दोआब
- सतलज-सरस्वती का दोआब, सरस्वती के लुप्त होने से अब सतलज-सरस्वती दोआब का अस्तित्व नहीं मिलता।

3.प्रायद्वीपीय पठार :-
भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर-पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची ( कार्डमम ) पहाड़ियों तथा उत्तर-पूर्व में शिलॉन्ग एवं कार्बा-एंगलोंग पठार तक है।इसकी औसत ऊँचाई 600-900 मीटर है। यह गोंडवानालैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था।
अत:यह प्राचीनतम भू-भाग पैंजिया का एक हिस्सा है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है।सामान्यतः प्रायद्वीप की ऊँचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन,चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर हैं जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपवाद हैं, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है।
प्रायद्वीपीय पठार को ‘ पठारों का पठार’ कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है।
- केंद्रीय उच्च भूमि,
- पूर्वी पठार,
- उत्तर-पूर्वी पठार,
- दक्कन का पठार

गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ ( उत्तर से दक्षिण के क्रम में )इस प्रकार हैं –
- कच्छ पहाड़ी
- मांडव पहाड़ी
- बरदा पहाड़ी
- गिरनार पहाड़ी
- गिर पहाड़ी
केंद्रीय उच्च भूमि
केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रो को शामिल किया जाता है-
- अरावली पर्वत श्रेणी
- मेंवाड का पठार
- मालवा का पठार
- विन्ध्यन श्रेणी
- बुंदेलखंड का पठार
- बुंदेलखंड का पठार
अरावली पर्वत श्रेणी :-
- अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर-पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण-पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किमी . है।
- यह प्राचीनतम मोड़दार ‘अवशिष्ट पर्वत’ ( Residual Mountain ) का उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति प्री-कैब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है
- अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य’जल विभाजक’ है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। ‘
- लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इसलिये यह एक अतः स्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है।
- अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी सहायक नदियाँ हैं।
- अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य जलवायु विभाजक भी हैं जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्द्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है।
- उत्तर-पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधनों, जैसे-तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर’गुरु शिखर’(722 मीटर ) है, जो’आबू पहाड़ी पर स्थित है। इसी आबू पहाड़ी में’जैनियों’का प्रसिद्ध धर्मस्थल’दिलवाड़ा जैन मंदिर’स्थित है जबकि अन्य शिखर’कुंभलगढ़’है।

मेवाड़ का पठार :-
- मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य पठार, अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है।
- यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। बनास नदी चंबल नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है।
मालवा का पठार :-
- मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को’मालवा का पठार’ कहते हैं। मालवा पठार को राजस्थान में’हाड़ौती का पठार’कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है।
- यहाँ बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, इसलिये मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिये उपयोगी है।
- चंबल, नर्मदा व ताप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे’बीहड़ या उत्खात भूमि’कहते हैं।
बुंदेलखंड का पठार :-
- इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है।
- इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सात जिले (जालौन,झाँसी,ललितपुर,चित्रकूट,हमीरपुर,बाँदा,महोबा ) तथा मध्य प्रदेश के सात जिले ( दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा ) आते हैं।
- यहाँ की ग्रेनाइट व नीस चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है।
- बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को ‘उत्खात भूमि का प्रदेश’कहते हैं।
- बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है।
- मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है।
विध्यन श्रेणी :-
- इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में ‘जोबट हिल’ और बिहार में ‘कैमूर हिल’ कहते हैं।
- विध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्यन पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है।
- विंध्यन श्रेणी, कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
- लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्त्व सबसे अधिक है।
- यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है।
सतपुड़ा श्रेणी :-
- यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटानागपुर के पठार तक है।
- यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है।
- इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी’धूपगढ़’( 1, 350 मी . ) है जो महादेव पर्वत पर स्थित है।
- मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी’अमरकंटक’( 1, 065 मी . ) है,यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है।
- यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण मुख्यत:ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है।
- यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जलविभाजक का कार्य करती है।
पूर्वी पठार :-
इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है-
- छोटानागपुर का पठार
- छत्तीसगढ़ बेसिन / महानदी बेसिन।
- दंडकारण्य का पठार
छोटानागपुर का पठार :-
- इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा, दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं।
- इस पठार के उत्तर-पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में राँची का पठार है। इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटानागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है।
- दामोदर नदी, राँची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। यह छोटानागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है।
- दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
- हजारीबाग पठार की चोटी ‘पारसनाथ हिल’ छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं।
- राँची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी, छोटानागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। राँची के समीप इस नदी पर ‘हुडरु जलप्रपात’ है।
- छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति। या द्वीप रूपीय स्थलाकृति को ‘पाट भूमि’ कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सट क्षेत्र एक ‘उत्थित भूखण्ड’ उदाहरण हैं।
छत्तीसगढ़ बेसिन / महानदी बेसिन :-
- छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन की प्रक्रिया द्वारा हुआ है।
- छत्तीसगढ़ बेसिन, छोटानागपुर के रॉची पठार को दण्डकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटानागपुर पठार के राँची पठार से अलग होता है।
- यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ-शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती हैं।
- छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है।
दंडकारण्य का पठार :-
- इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है। अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है।
- यह अत्यंत ही ऊबड़-खाबड़ एवं अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- गोदावरी की सहायक नदी ‘इंद्रावती’ का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है।
- भारत में ‘टिन धातु’ दंडकारण्य पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है।
उत्तर-पूर्वी पठार :-
मेघालय का पठार :-
- उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार ( छोटानागपुर का पठार ) का ही पूर्वी विस्तार है, जो ‘राजमहल-गारो गैप’ अथवा ‘मालदा गैप’ के द्वारा अलग हुआ है।
- इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं।
- गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं।
- खासी पर्वतीय क्षेत्र का’कीप’रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के। कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित’मॉसिनराम’एवं’चेरापूंजी’विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं।
- यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित’शिलॉन्ग रेंज’सबसे ऊँचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिये इसे’शिलॉन्ग के पठार’के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी ‘नॉकरेक’ ( मेघालय में अवस्थित ) है।
- औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ ‘लैटेराइट मिट्टी’ तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है।
मालदा गैप या राजमहल-गारो गैप :-
- इसकी उत्पत्ति’प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धंसाव की प्रक्रिया’के कारण हुई है।
- इसके द्वारा छोटानागपुर का राजमहल पर्वत, मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिये इसे’राजमहल-गारो गैप’कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे’मालदा गैप’कहते हैं।
- गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा / राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है।
- इस डेल्टाई मैदान में’पीट मृदा’की उपलब्धता के कारण ही’मैंग्रोव वनस्पत’का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला’सुंदरबन’भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है।
दक्कन का पठार :-
इस पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है।
- दक्कन ट्रैप
- कर्नाटक का पठार
- आंध्र का पठार
दक्कन टैप :-
- महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ’काली मिट्टी का विकास हुआ है इसलिये यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
- इसका विस्तार 16º उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर-पूर्व में नागपुर तक है।
- इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है।
- सतमाला,अजंता,बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है।
कर्नाटक का पठार :-
- कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को ‘मलनाड’ कहते हैं।’बाबा बूदान’यहाँ का सबसे ऊँचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा ‘मुल्लयानगिरी’ ( मुलनगिरी ) इसकी सबसे ऊँची चोटी है। ( ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बाबा बूदान की सबसे ऊँची चोटी दर्शाया गया है। )
- मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊँचे पठारी क्षेत्र को ‘मैदान’कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊँचे मैदानी क्षेत्र को ‘बंगलूरू का पठार’एवं ‘मैसूर का पठार’ के नाम से जाना जाता है।
- कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
- यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिये बाबा बूदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है।
- कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्त्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे ‘जोग या गरसोप्पा’ जलप्रपात कहते हैं। इसे ‘महात्मा गांधी’ जलप्रपात भी कहते हैं।
- कुंचीकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात ( 455 मीटर ) है, जो कि शिमोगा जिले ( कर्नाटक ) में’वाराही नदी’पर है। ( वर्तमान स्रोतों के आधार पर )।
आंध्र का पठार :-
- आंध्र के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठार तथा तेलंगाना के पठार’को शामिल किया जाता है।
- कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, जहाँ वेलीकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं।
- तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है।
- कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में ‘कोल्लेरू झील’ अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है।
दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र :-
- दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आदि आती हैं।
- डोडाबेटा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है, जबकि माकुर्ती ( Makurti ) इसकी दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल’उडगमंडलम या ऊटी’नीलगिरी में ही अवस्थित है।
- अन्नामलाई पर्वत की चोटी’अनाईमुडी’( 2695 मी . ) दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है, जबकि कार्डमम, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है।
- नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच’पालघाट दर्रा स्थित है, जो पल्लकड़ को कोयंबटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच’सेनकोटा दर्रा’अवस्थित है, जो’तिरुवनंतपुरम को’मदुरै’से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल’कोडाईकनाल’पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है।
- केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी ( Silent Valley ) सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है।
पश्चिमी घाट :-
- पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1,600 कि . मी . की लंबाई में है।
- पश्चिमी घाट को’सह्याद्रि’भी कहा जाता है, इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई लगभग 1,000-1,300 मीटर है। महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं।
- यह उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने ( महाराष्ट्र-गुजरात की सीमा ) से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है।
- इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है , जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है।
- महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख ( एश्चुअरी ) का निर्माण करती है।
- पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को’विश्व धरोहर स्थल’घोषित किया था।

| प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे | ||
| थाल घाट दर्रा | महाराष्ट्र | मुंबई-नासिक |
| भोर घाट दर्रा | महाराष्ट्र | मुंबई-पुणे |
| पाल घाट दर्रा | केरल | पलक्कड़-कोयंबटूर(नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य) |
| सेनकोटा गैप | केरल | तिरुवनंतपुरम्-मदुरै |
पूर्वी घाट :-
- भारत का पूर्वी घाट एक असतत् श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है।
- गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊँचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ( लगभग 1, 100 मी . ) है।
- पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलीकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहा जाता है।
- पूर्वी घाट में कॅटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है जिसे जवादी, शेवरॉय आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है जो अंत में नीलगिरी में मिल जाते हैं।

पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम ( उत्तर से दक्षिण ) :-
आंध्र प्रदेश
- नल्लामलाई पहाड़ी
- वेलीकोंडा पहाड़ी
- पालकोंडा पहाड़ी
- नगारी पहाडी
तमिलनाडु
- जवादी पहाड़ी
- शेवरॉय पहाड़ी
- पंचमलाई पहाड़ी
- सिरुमलाई पहाड़ी
4 भारत के तटीय मैदान :-
भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी ( पूर्वी एवं पश्चिमी घाट ) तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है।
भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है-
1.पश्चिमी तटीय मैदान 2.पूर्वी तटीय मैदान

पश्चिमी तटीय मैदान :-
पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है।
पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः चार वर्गों में बाँटा जाता है-
- गुजरात का मैदान या तट-गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र ( इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं )।
- कोंकण का मैदान तट-दमन (महाराष्ट्र) से गोवा के बीच।
- कन्नड का मैदान या तट-गोवा से मंगलूरू के बीच।
- मालाबार का मैदान या तट-मंगलूरू एवं कन्याकुमारी ( केप कॉमोरिन ) के बीच।
- भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है लेकिन केरल में यह पुन:चौड़ा हो जाता है।
- कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है।
- कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है।
- मालाबार के तटीय मैदान में कयाल ( लैगून ) पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ-साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है।
- केरल के बेम्बनाद कयाल में प्रतिवर्ष’नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली ( नौका दौड ) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
- पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं और यह अधिक कटा-फटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिये प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।
पूर्वी तटीय मैदान :-
पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को’पूर्वी तटीय मैदान’कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है।
पूर्वी तटीय मैदान या घाट को तीन भागों में बाँटा जाता है-
- उत्कल तट-स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच ( ओडिशा )
- उत्तरी सरकार तट-महानदी से कृष्णा नदी के बीच ( ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश )
- कोरोमंडल तट-कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच ( आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु )
- पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-पूर्वी मानसून, दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है।
- इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक की जाती है।
- पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोल्लेरू झील स्थित है।
- चिल्का व पुलिकट लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं।
- पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर एश्चुअरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं।
पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित हैं-
- महानदी डेल्टा – ओडिशा
- गोदावरी डेल्टा – आंध्र प्रदेश
- कृष्णा डेल्टा – आंध्र प्रदेश
- कावेरी डेल्टा – तमिलनाडु
5.भारत के द्वीप समूह :-
- भारत में लगभग कुल 1000 से अधिक द्वीप है।
- मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है-
- अण्डमान निकोबार द्वीप समुह(बंगाल की खाड़ी में)
- लक्ष्यद्वीप समूह(अरब सागर)
क्षेत्रफल तथा आबादी दोनों की दृष्टि से अण्डमान निकोबार लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है।

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह :-
- यहां लगभग 350 द्वीप है(केवल 38 पर मानव रहते हैं।)
- अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल चोटी(उत्तरी अंडमान, 738 मी) है।
- इसी द्वीप में स्थित एक द्वीप ‘बैरन द्वीप’ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
- भारत का दक्षिण बिन्दु ‘इंदिरा प्वाइंट’ जो ग्रेट निकोबार में स्थित है।
- 10º चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है।
- डंकन दर्रा दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के बीच है।

लक्षद्वीप समूह :-
- यह मुख्य भूमि के पश्चिमी तट से 220-240 किमी. की दूरी पर अरब सागर में स्थित है।
- इसमें कुल 36 द्वीप है(केवल 10 पर मानव) रहते हैं।
- अगान्ती यहां एक मालद्वीप है जहां हवाई अड्डा है।
- ‘एण्ड्रोट’ लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा(4,90 किमी.) द्वीप है।
- ‘टूना’ यहां पकड़ी जाने वाली प्रमुख मछली है।
- यहां स्थित सभी द्वीपों में मलयालम(मिनिकाय द्वीप एक मात्र अपवाद यहां महल भाषा) बोली जाती है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 94.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है।
- यहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है।

अन्य प्रमुख भारतीय द्वीप :-
पम्बन द्वीप– यह मन्नार की खाड़ी में है। यह आदम ब्रिज का भाग है।

श्रीहरिकोटा द्वीप – आन्ध्र प्रदेश के समीप पुलीकट झील के अग्र भाग में अवस्थित।

न्यू मूर द्वीप – बंगाल की खाड़ी में भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है।